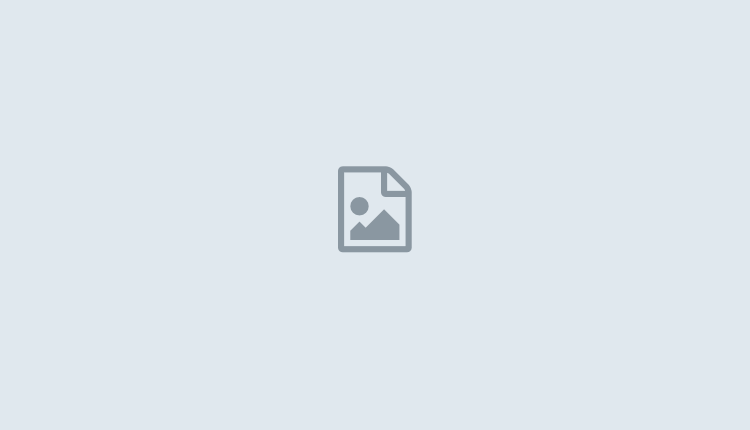सुशील उपाध्याय
मोटे तौर पर देखें तो हिंदी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री की मंशा पर सवाल उठाने की कोई ठोस वजह नहीं है, लेकिन उनके बयान का जिस तरह से देश के कई हिस्सों में विरोध हुआ, वो बात ध्यान देने वाली है। मेरे एक मलयाली मित्र हैं, जो हिंदी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर कई ऐसी बातें कहीं जो हिंदीभाषी, विशेष रूप से उत्तर भारतीय लोगों के जेहन में नहीं आती। मसलन, भले ही हिंदी वाले कुछ भी दावा करें, लेकिन जनगणना का आंकड़ा यह बताता है कि देश में उन लोगों की संख्या 40 फीसद से थोड़ा सी ज्यादा है, जिन्होंने हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया हुआ है। इसके अलावा वे लोग काफी संख्या में हैं जो हिंदी बोल और समझ लेते हैं, लेकिन जिनकी मातृभाषा हिंदी से अलग है। इन लोगों में पंजाबी, गुजराती, मराठी, कुछ हद तक बांग्ला, असमिया और नेपाली बोलने वाले लोगों को भी सम्मिलित कर सकते हैं।
इसे और विस्तार देना चाहे तो कह सकते हैं कि भारत के सर्वाधिक आबादी वाले 10 बड़े शहरों में से चेन्नई को छोड़ दीजिए तो गैर हिंदीभाषी मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद अहमदाबाद, गुवाहाटी बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम आदि में भी बड़ी संख्या में हिंदी बोलने और समझने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन ये जबरन हिंदी वाले नहीं हैं। और यदि इन किसी पहचान का दबाव बनाया जाएगा तो ये हिंदी के साथ नहीं, बल्कि अपनी मातृभाषा के साथ खड़े होंगे।
इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि बीते 50 साल में और विशेष रूप से बीते 30 साल में हिंदी बोलने वालों की संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस बढोत्तरी में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी से अलग है, लेकिन उन्हें नौकरी, कारोबार आदि के कारण हिंदीभाषी लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। इसलिए ये हिंदी में भी आसानी से व्यवहार कर लेते हैं। अब सवाल यह है जब देश के गृहमंत्री हिंदी को अंग्रेजी का विकल्प बनाने की बात कहते हैं तो पश्चिम बंगाल से आने वाले कांग्रेसी नेता अधीर रंजन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के अलावा तेलंगाना, आंध्र और असम से भी विरोध में आवाज क्यों उठने लगी। मेरे मित्र बताते हैं कि ये आवाज हिंदी के विरोध में नहीं है, बल्कि ये उस सोच के विरोध में है जो हिंदी श्रेष्ठता-बोध के चलते अंग्रेजी की जगह हिंदी को लाना चाहती है। गैर हिंदीभाषी क्षेत्र के लोगों के लिए इसका अर्थ यह है कि वे अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाने के लिए बाध्य होंगे। उनका यह भी कहना है कि हिंदी पट्टी के बाहर हिंदीभाषी लोगों का व्यवहार लगभग वैसा ही है, जैसा कि अंग्रेजीभाषी लोगों का है। दोनों ही आधिपत्य का चरित्र रखती हैं। हिंदीभाषी मानते हैं कि देश के हर आदमी को उनसे हिंदी में ही बात करनी चाहिए और जो हिंदी नहीं जानता वह इस देश का प्रथम श्रेणी का नागरिक नहीं है। परिणामतः जैसे ही हिंदी को लेकर सरकारी स्तर पर कोई सर्वजनिकनबात होती है, तुरंत विरोध के स्वर खड़े हो जाते हैं जबकि ग्राउंड लेवल पर हिंदी का काफी काम हो रहा है।
तमिलनाडु को अपवाद मान लें तो देश का कोई ऐसा गैर हिंदीभाषी प्रदेश नहीं है, जहां हिंदी को प्राथमिकता के आधार पर न पढ़ाया जा रहा हो। मेरे मित्र सवाल करते हैं कि हिंदी पट्टी में कोई एक ऐसा राज्य बताइए, जहां उसी तरह से देश की कोई अन्य भाषा पढ़ाई जा रही हो जैसे कि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में स्कूल स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती है। वास्तव में यह तर्क काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी पट्टी का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां प्री-प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी यानी दसवीं क्लास तक दक्षिण भारत अथवा पूर्वोत्तर भारत की कोई भी भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जा रही हो।
तो फिर सवाल यह है कि दक्षिण भारतीय अथवा पूर्वोत्तर के लोगों के लिए यह मजबूरी क्यों हो कि वे अंग्रेजी छोड़ कर हिंदी को पढ़ें और यदि त्रिभाषा फार्मूला के अंतर्गत गैर हिंदीभाषी क्षेत्रों में हिंदी को अनिवार्य किया जाना है तो फिर यही बात हिंदी पट्टी पर भी लागू होनी चाहिए कि उन्हें तीसरी भाषा के रूप में पहली से लेकर दसवीं क्लास तक देश की कोई अन्य महत्वपूर्ण भाषा पढ़नी चाहिए। पूरी दुनिया में, खासतौर से यूरोप में ऐसी बहुत बड़ी आबादी है जो 3-4 भाषाओं तक में अपना दैनिक व्यवहार करती है। यही बात भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों के लोगों के बारे में भी कही जा सकती है। इन राज्यों की आबादी में से ज्यादातर लोग तीन या अधिक भाषाएं जानते हैं, लेकिन उत्तर भारत के मामले में यह बात लागू नहीं होती। यहां हिंदी जानने वाला सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर तक अंग्रेजी तो पढ़ता है लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं के नाम पर वह संस्कृत या इक्का-दुक्का जगहों पर पंजाबी, उर्दू की पढ़ाई कर लेता है। और इसी से उसका दायित्व पूरा हुआ मान लिया जाता है।
न केवल मेरे मलयाली प्रोफेसर मित्र, बल्कि दक्षिण भारत के अन्य हिंदीप्रेमी लोगों का भी यही अनुभव है कि जब भी सत्ता शीर्ष से हिंदी को लागू करने अथवा उसे किसी अन्य भाषा के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करने की बात होगी तो खुला विरोध होगा ही। वजह बहुत साफ है, चाहे पश्चिम बंगाल के लोग हों अथवा तमिलनाडु या केरल के, ये सभी सांस्कृतिक रूप से प्रबुद्ध होने के साथ-साथ अपनी भाषा एवं संस्कृति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील भी हैं। इस कारण हिंदी से जुड़ा कोई भी प्रस्ताव या घोषणा उन्हें असहज करती है। जहां तक हिंदी को अंग्रेजी का विकल्प बनाने की बात है तो इस बात में तथ्यात्मक रूप से कोई गंभीरता परिलक्षित नहीं होती। तीन दशक पहले देश में नई आर्थिक नीतियां लागू होने के बाद जिस तेजी से अंग्रेजी का शिक्षण बढ़ा है, उस लिहाज से अगले 20-25 साल में अंग्रेजी देश में दूसरी सबसे बड़ी भाषा बनने की ओर बढ़ रही है।
भारत सरकार के सहयोग से संचालित केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल, केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल, इन सभी में अंग्रेजी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जा रही है। उत्तर भारत में अब केवल शहरों में नहीं, बल्कि गांवों तक मे अंग्रेजी पढ़ने और सीखने का सिलसिला उन्माद के स्तर तक बढ़ा हुआ है। ऐसा आकर्षण देश में शायद ही किसी अन्य भाषा को लेकर हो। इसके पीछे मूल वजह यही है कि लोगों को लगता है कि अंग्रेजी सीख-पढ़कर रोजगार पाने की संभावना को बेहतर किया जा सकता है। साथ ही यह भाषा दुनिया के साथ जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी है। और इन सब के साथ इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अंग्रेजी भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है इसलिए अंग्रेजी को विदेशी भाषा के रूप में चिन्हित करने और प्रचारित करने का कोई तार्किक कारण मौजूद नहीं है। वस्तुतः जिस दिन उत्तर भारत के लोग दक्षिण और पूर्वोत्तर की भाषाओं को एक अभियान की तरह सीखने लगेंगे, उस दिन वास्तव में उनके पास ऐसे लोगों को जवाब देने का नैतिक अधिकार होगा जो हिंदी का विरोध करते हैं।